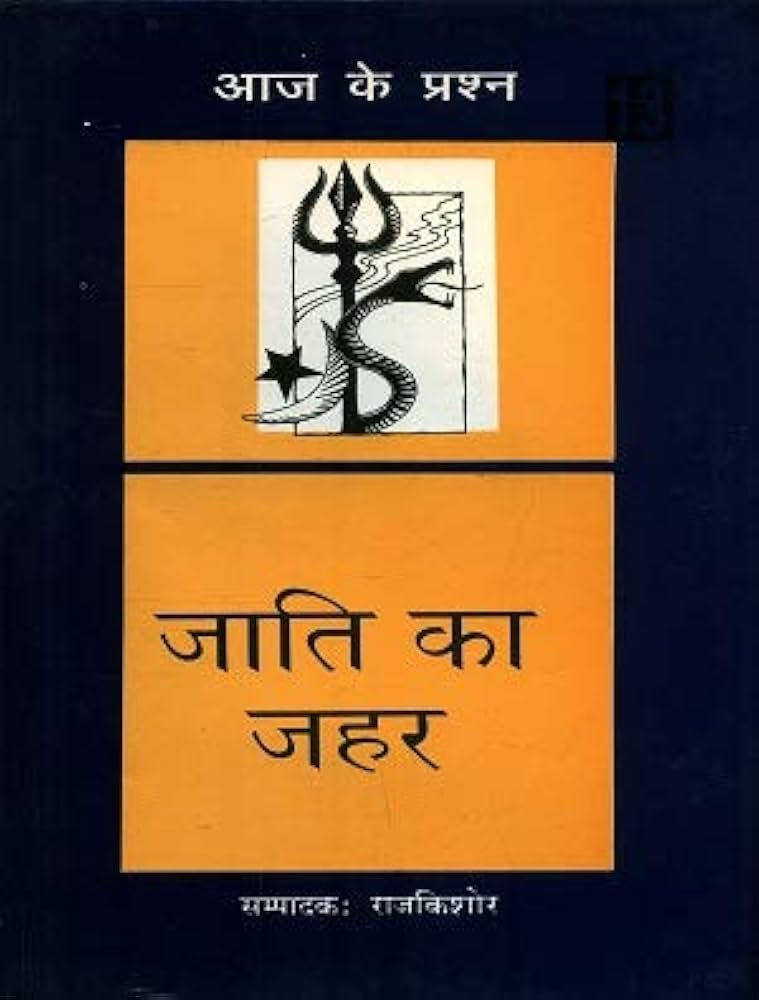
अहंकार और घृणा में इतने डूबे हों कि वे या तो संविधान निर्माता को “
गंदा” कहने का दुस्साहस करें या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने जैसी शर्मनाक हरकत करें — तब समझना चाहिए कि समाज की आत्मा बीमार हो चुकी है।डॉ. आंबेडकर ने कहा था
— मनुष्य की असमानता ही भारत की सबसे बड़ी बीमारी है।आज यह बीमारी फिर सिर उठा रही है। फर्क बस इतना है कि यह अब खुलेआम, अभिमान के साथ प्रकट हो रही है — और दुख की बात यह है कि इसमें कोई शर्म नहीं, बल्कि “सामाजिक समर्थन” का आभास झलकता है।यह सवाल बेहद जरूरी है —
क्या जातिवाद खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ जाति के पीड़ितों की है?क्या बराबरी की लड़ाई सिर्फ वही लड़ेंगे जिनके हिस्से सदियों का अपमान आया?अगर उच्च कही जाने वाली जातियाँ मौन रहेंगी, अगर सत्ता-संरचना “संवेदनशील” होने के बजाय
“संवेदनहीन” बनी रहेगी — तो यह मौन भी अपराध है।दलित व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़-लिख ले, कितनी भी ऊँचाई पर पहुँच जाए — समाज उसकी “काबिलियत” नहीं, उसकी “जाति” देखता है। यही कारण है कि कोई जज, कोई अफसर, कोई वकील — सबको बार-बार अपनी “पहचान” याद दिलाई जाती है।
यह वही व्यवस्था है जो “न्याय” को “न्यायपालिका” से बाहर निकालकर “जाति” के बक्से में बंद कर देती है।आज का भारत अपनी आत्मा पर प्रश्न खड़ा कर रहा है —क्या यह वही देश है जो समानता के मूल्यों पर टिका था, या फिर वही पुराना भारत है जो बस ऊँची इमारतों में छिपे अपने भेदभाव को आधुनिकता का आवरण पहना रहा है?इन दो घटनाओं को किसी “व्यक्तिगत उग्रता” की तरह नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी के रूप में देखना चाहिए।
यह चेतावनी है कि जाति का ज़हर अब न्याय की कुर्सी और संविधान की आत्मा तक पहुँच चुका है।और अगर हम इस पर आज भी चुप रहे — तो कल शायद संविधान की गरिमा पर नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व पर ही जूता फेंका जाएगा।



